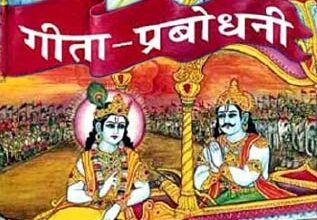धर्मक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे (पन्द्रहवां अध्याय-06)
सूर्य का प्रकाश व पोषणशक्ति भगवान का अंश

रामायण अगर हमारे जीवन में मर्यादा का पाठ पढ़ाती है तो श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। द्वापर युग के महायुद्ध में जब महाधनुर्धर अर्जुन मोहग्रस्त हो गये, तब उनके सारथी बने योगेश्वर श्रीकृष्ण ने युद्ध मैदान के बीचोबीच रथ खड़ाकर उपदेश देकर अपने मित्र अर्जुन का मोह दूर किया और कर्तव्य का पथ दिखाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने छोटे-छोटे राज्यों में बंटे भारत को एक सशक्त और अविभाज्य राष्ट्र बनाया था। गीता में गूढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है। श्री जयदयाल गोयन्दका ने यह जनोपयोगी कार्य किया। उन्होंने श्रीमद भागवत गीता के कुछ गूढ़ शब्दों को जन सामान्य की भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि गीता को जन सामान्य भी अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतार सके।-प्रधान सम्पादक यदादित्यगतं तेजो जग˜ासयतेऽखिलम्।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्।। 12।।
प्रश्न-‘आदित्यगतम्’ विशेषण के सहित ‘तेजः’ पद किसका वाचक है और वह समस्त जगत् को प्रकाशित करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है?
उत्तर-सूर्य मण्डल में जो एक महान् ज्योति है, उसका वाचक यहाँ आदित्यगतम् विशेषण के सहित तेजः पद है और वह समस्त जगत् को प्रकाशित करता है यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि स्थूल संसार की समस्त वस्तुओं को एक सूर्य का तेज ही प्रकाशित करता है।
प्रश्न-चन्द्रमा में और अग्नि में स्थित तेज किसका वाचक है और उन तीनों में स्थित तेज को तू मेरा ही तेज समझ इस कथन का क्या अभिप्राय है?
उत्तर-चन्द्रमा मे जो ज्योत्सना है उसका वाचक चन्द्रस्थ तेज है एवं अग्नि में जो प्रकाश है, उसका वाचक अग्निस्थ तेज है। इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि में स्थित समस्त तेज को अपना तेज बतलाकर भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि उन तीनों में और वे जिनके देवता हैं-ऐसे नेत्र, मन और वाणी में वस्तु को प्रकाशित करने की जो कुछ भी शक्ति है-वह मेरे ही तेज का एक अंश है जबकि इन तीनों में स्थित तेज भी मेरे ही तेज का अंश है, तब जो इन तीनों के सम्बन्ध से तेज युक्त कहे जाने वाले अन्यान्य पदार्थ हैं-उन सबका तेज तेरा ही तेज है, इसमें तो कहना ही क्या है। इसीलिये छठे श्लोक में भगवान् ने कहा है कि सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि ये सब मेरे स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हैं।
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा।
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः।। 13।।
प्रश्न-मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त भूतों को धारण करता हूँ इस कथन का क्या भाव है?
उत्तर-इस कथन से भगवान् पृथ्वी को उप लक्षण बनाकर विश्व व्यापिनी धारण शक्ति को अपना अंश बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वी में जो भूतों को धारण करने की शक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार और किसी में जो धारण करने की शक्ति है-वह वास्तव में उसकी नहीं, मेरी ही शक्ति का एक अंश है। अतएव मैं स्वयं ही आत्मरूप से पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने बल से समस्त प्राणियों को
धारण करता हूँ।
प्रश्न-‘रसात्मकः’ विशेषण के सहित ‘सोमः’ पद किसका वाचक है और इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है?
उत्तर-रस ही जिसका स्वरूप हो, उसे रसात्मक कहते हैं अतएव रसात्मक विशेषण के हित सोमः पद चन्द्रमा का वाचक है और यहाँ सोमः के साथ रसात्मकः विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि चन्द्रमा का स्वरूप रसमय-अमृतमय है तथा वह सबको रस प्रदान करने वाला है।
प्रश्न-ओषधीः पद किसका वाचक है और मैं ही चन्द्रमा बनकर समस्त ओषधियों को पुष्ट करता हूँ इस कथन का क्या अभिप्राय है?
उत्तर-ओषधीः पद पत्र, पुष्प और फल आदि समस्त अंग-प्रत्यंगों के सहित वृक्ष, लता और तृण आदि जिनके भेद हैं-ऐसी समस्त वनस्पतियों का वाचक है तथा मैं ही चन्द्रमा बनकर समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ इससे भगवान् ने यह दिखलाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमा में प्रकाशन शक्ति मेरे ही प्रकाश का अंश है, उसी प्रकार जो उसमें पोषण करने की शक्ति है-वह भी मेरी ही शक्ति का एक अंश है, अतएव मैं ही चन्द्रमा के रूप में प्रकट होकर सबका पोषण करता हूँ।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।। 14।।
प्रश्न-यहाँ प्राणिनां देहमाश्रितः विशेषण के सहित वैश्वानरः पद किसका वाचक है और मैं प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर बनकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, भगवान् के इस कथन का क्या अभिप्राय है?
उत्तर-जिसके कारण सबके शरीर में गरमी रहती है और अन्न का पाक होता है समस्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले उस अग्नि का वाचक यहाँ प्राणिनां देहमाश्रितः विशेषण के सहित वैश्वानरः पद है तथा भगवान् ने मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अग्नि की प्रकाश शक्ति मेरे ही तेज का अंश है, उसी प्रकार उसका जो उष्णत्व है अर्थात् उसकी जो पाचन, दीपन करने की शक्ति है वह भी मेरे ही शक्ति का अंश है। अतएव मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले वैश्वानर अग्नि के रूप में भव्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य पदार्थों को अर्थात् दाँतों से चबाकर खाये जाने वाले रोटी, भात आदि निगलकर खाये जाने वाले रबड़ी,
दूध, पानी आदि चाटकर खाये जाने वाले शहद, चटनी आदि और चूसकर खाये जाने वाले ऊख आदि ऐसे चार प्रकार के भोजन को पचाता हूँ।
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।
वेदैश्व सवैंरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।। 15।।
प्रश्न-मैं सबके हृदय में स्थित हूँ इस कथन का क्या अभिप्राय है?
उत्तर-इससे भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि मैं सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण हूँ फिर भी सबके हृदय में अन्तर्यामी रूप से मेरी विशेष स्थिति है अतएव हृदय मेरी
उपलब्धि का विशेष स्थान है। इसीलिये मैं सबके हृदय में स्थित हूँ ऐसा कहा जाता है क्योंकि जिनका अन्तःकरण शुद्ध और स्वच्छ होता है, उनके हृदय में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है।
प्रश्न-‘स्मृति’ ज्ञान और अपोहन शब्दों का अर्थ क्या है और ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान् ने क्या भाव दिखलाया है?
उत्तर-पहले देखी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या घटनादि के स्मरण का नाम ‘स्मृति’ है। किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है। तथा संशय, विपर्यय आदि वितर्क जाल का वाचक ऊहन है और उसके दूर होने का नाम अपोहन है। ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि सबके हृदय में स्थित मैं अन्तर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियों के कर्मानुसार उपर्युक्त स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावों को उनके अन्तःकरण में उत्पन्न करता हूँ। -क्रमशः (हिफी)