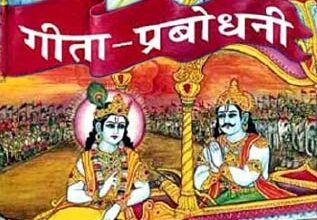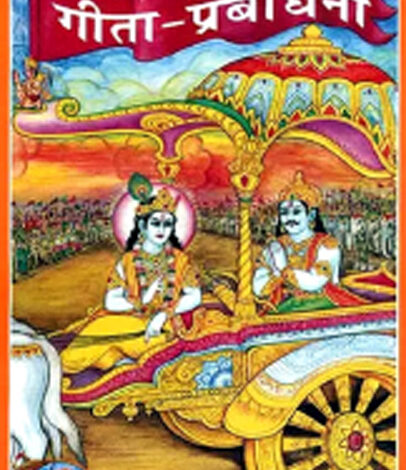
(हिफी डेस्क-हिफी फीचर)
जिस तरह मर्यादा पुुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र को लेकर कहा गया है कि ‘हरि अनंत हरि कथा अनंता…’ उसी प्रकार भगवान कृष्ण के मुखार बिन्दु से प्रस्फुटित हुई श्रीमद् भगवत गीता का सार भी अतल गहराइयों वाला है। विद्वानों ने अपने-अपने तरह से गीता के रहस्य को समझने और समझाने का प्रयास किया है। गीता का प्रारंभ ही जिस श्लोक से होता है उसकी गहराई को समझना आसान नहीं है। कौरवों और पांडवों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वह भी धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म भूमि और कुरु क्षेत्रे अर्थात तीर्थ भूमि पर लड़ा गया जिससे युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वालों का कल्याण हो गया। इसी तरह की व्याख्या स्वामी रामसुख दास ने गीता प्रबोधनी में की है जिसे हम हिफी के पाठकों के लिए क्रमशः प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। हम स्वामी जी के आभारी हैं जिन्होंने गीता के श्लोकों की सरल शब्दों में व्याख्या की है। -प्रधान सम्पादक
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात्।
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।। 7।।
हे पार्थ! मुझमें आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्युरूप संसार-समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला जाना जाता हूँ।
व्याख्या-छठे अध्याय के पाँचवें श्लोक में भगवान् ने सामान्य साधकों के लिये अपने द्वारा उद्धार करने की बात कही थी। ‘उद्धरेदात्मनात्मानम्’ और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरम्भ में स्वयं ही साधन में लगता है परन्तु जो साधक भगवान् के आश्रित होता है, उसका उद्धार भगवान् करते हैं। वह तो अपने उद्धार की चिन्ता न करके केवल भगवान् के भजन में ही लगा रहता है। उसका साधन और साध्य भगवान् ही होते हैं। परन्तु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है।
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।। 8।।
तू मुझमें मन को स्थापित कर और मुझमें ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझमें ही निवास करेगा-इसमें संशय नहीं है।
व्याख्या-मन बुद्धि भगवान् की अपरा प्रकृति है (गीता 7/4-5)। भगवान् की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान् से भिन्न स्वभाववाली (जड़ और परिवर्तनशील) है। परन्तु परा प्रकृति (जीवात्मा) भगवान् से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिये वास्तव में मन-बुद्धि भगवान् में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान् में लग सकता है। गीता में जहाँ-जहाँ मन-बुद्धि भगवान् में लगाने की बात आयी है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान् में लगाने की बात कही गयी है।
भगवान् में मन-बुद्धि लगाने से मन-बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है-‘निवसिष्यसि मय्येव’। कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वहीं लगता है, जहाँ उसके मन-बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है, धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन-बुद्धि जहाँ जाते हैं, स्वयं वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ सम्बन्ध जोड़ने से मन-बुद्धि संसार में लग गये। संसार में मन-बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसलिये जीव को संसार से हटाने के लिये भगवान् मन-बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं।
भगवान् में लगाने से मन-बुद्धि भगवान् में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान् का ही स्वभाव है। भगवान् में लीन होने पर मन-बुद्धि की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान् ही रह जाते हैं।
पूर्व पक्ष-मन-बुद्धि तो करण हैं, पर जीव कर्ता है। करण कर्ता के अधीन रहते हैं। जहाँ कर्ता लगेगा, वहीं करण भी लगेंगे। अतः जहाँ करण लगेंगे, वहां कर्ता भी लगेगा-ऐसा कहने का क्या औचित्य है?
उत्तर पक्ष-क्रिया की सिद्धि में करण अत्यन्त उपकारक होता है-‘साधकतमं करणम्’ (पाणि0 अ0 1/4/42) जैसे, राम के बाण से बालि मारा गया–इस वाक्य में ‘बाण’ करण है, क्योंकि बालि के मरने में बाण हेतु हुआ, धनुष, प्रत्यंचा, हाथ आदि नहीं। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ करण ‘बुद्धि’ है, जिससे वह परमात्मा में लगाता है। उपनिषद् में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इन्द्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथि कहा गया है-‘बुद्धिं तु सारथिं विद्धि (कठोप निषद् 1/3/3)। रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर रनिवास तक सारथि जाता है। फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है, सारथि लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुँचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा तक स्वयं ही पहुँच पाता है।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम््।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय।। 9।।
अगर तू मन को मुझमें अचल भाव से स्थिर ़(अर्पण) करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय! अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर।
व्याख्या-एकमात्र भगवत्प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम-जप आदि ‘अभ्यास योग’ है। यदि केवल अभ्यास हो, योग न हो तो एक नयी स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार-बार भगवान् में लगाना अभ्यास है (गीता 6/26)। परन्तु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से सम्बन्ध-विच्छेद है।
अभ्याससेऽप्यसमर्थोऽसि तम्कर्मपरमो भव।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि।। 10।।
अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिये कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिये कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जायगा।
व्याख्या-अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान् के अर्पण करना सुगम है। कारण कि अभ्यास तो नया काम है, जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं। उन लौकिक-पारमार्थिक सभी कर्मों को भगवान् के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान् को प्राप्त हो जाता है (गीता 9/27-28)।
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।। 11।।
अगर मेरे योग (समता) के आश्रित हुआ तू इस (पूर्व श्लोक में कहे गये साधन) को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन-इन्द्रियों को वश में करके सम्पूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर।
व्याख्या-यदि साधक सम्पूर्ण कर्मों को भगवान् के अर्पण न कर सके अर्थात् भगवान् के लिये सभी कर्म न कर सके तो उसे फलेच्छा त्याग करके कर्तव्य-कर्म करने चाहिये, क्योंकि फलेच्छा ही बाँधने वाली है-‘फले सक्तो निबध्यते’ (गीता 5/12)। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य-कर्म करने से उसका संसार से सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा।-क्रमशः (हिफी)