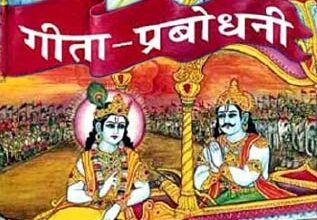श्रीमद् भगवत गीता का प्रबोध-98
जिस तरह मर्यादा पुुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र को लेकर कहा गया है कि ‘हरि अनंत हरि कथा अनंता…’ उसी प्रकार भगवान कृष्ण के मुखार बिन्दु से प्रस्फुटित हुई श्रीमद् भगवत गीता का सार भी अतल गहराइयों वाला है। विद्वानों ने अपने-अपने तरह से गीता के रहस्य को समझने और समझाने का प्रयास किया है। गीता का प्रारंभ ही जिस श्लोक से होता है उसकी गहराई को समझना आसान नहीं है। कौरवों और पांडवों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वह भी धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म भूमि और कुरु क्षेत्रे अर्थात तीर्थ भूमि पर लड़ा गया जिससे युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वालों का कल्याण हो गया। इसी तरह की व्याख्या स्वामी रामसुख दास ने गीता प्रबोधनी में की है जिसे हम हिफी के पाठकों के लिए क्रमशः प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। हम स्वामी जी के आभारी हैं जिन्होंने गीता के श्लोकों की सरल शब्दों में व्याख्या की है। -प्रधान सम्पादक
गीता सुनने मात्र से ही शुभ लोकों की प्राप्ति
य इदं परमं गुह्यं म˜क्तेष्वभिधास्यति।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः।। 68।।
मुझमें परा भक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद (गीता ग्रन्थ) को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है।
व्याख्या-जो केवल भगवान् की भक्ति का उद्देश्य रखकर निःस्वार्थ भाव से इस परम गोपनीय गीता को भक्तों में सुनाता है, वह भगवान् को प्राप्त होता है। जो भोजन-शयन, शौच-स्नान आदि शारीरिक क्रियाओं को भी भगवान् को अर्पित कर देता है, वह भी भगवान् को प्राप्त हो जाता है (गीता 9/27-28) फिर जो केवल भगव˜क्ति का उद्देश्य रखकर भगवद्वाणी (गीता) का प्रचार करता है, वह भगवान् को प्राप्त हो जाय, इसमें कहना ही क्या है।
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।। 69।।
उसके समान मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमण्डल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी
नहीं।
व्याख्या-जिसका एकमात्र भगवत्प्राप्ति का, भगवत्प्रेम का ही उद्देश्य है, जो गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। ऐसा साधक ही भगवान् का अत्यन्त प्रिय कार्य (गीता-प्रचार) करने वाला है। जो लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी-मण्डल पर भगवान् का दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। कारण कि शिखा से मनुष्य मात्र प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। गीता ने युद्ध-जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है (गीता 2/38, 9/27, 18/46 आदि)। जब युद्ध-जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, फिर अन्य परिस्थिति में कैसे नहीं होगा? इसलिये भगवान् गीता के प्रचार की विशेष महिमा गाते हैं।
जो मनुष्य भगवान् का अत्यन्त प्रिय हो जाता है, उसे ज्ञान-योग, कर्म योग और भक्तियोग-तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं।
अध्येष्यते च य इमं धम्र्यं संवादमावयोः।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।। 70।।
जो मनुष्य ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं (गीता 4/33)। जो गीता का अध्ययन करता है, उसके द्वारा भगवान् ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, फिर उसके अनुसार आचरण करने का कितना माहात्म्य होगा।
श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः।
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्।। 71।।
श्रद्धावान् और दोषदृष्टि से रहित जो मनुष्य (इस गीता ग्रन्थ को) सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्यकारियों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जायगा।
व्याख्या-गीता की बातों को जैसा सुन ले, उसे प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा-का-वैसा मानने वाले का नाम ‘श्रद्धावान’ है, और उन बातों में कहीं भी, किसी भी विषय में किंचिन्मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम ‘अनसूयः’ है। ऐसा श्रद्धावान् तथा दोषदृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर पुण्यकारियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है।
श्रद्धा-भक्ति के तारतम्य से गीता के सुनने में तारतम्य रहता है, और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्गादि लोकों से लेकर भगवल्लोक तक अधिकार हो जाता है। तात्पर्य है कि श्रोता में अधिक श्रद्धा-भक्ति होगी तो वह भगवान् के परमधाम को प्राप्त हो जायगा, और कम श्रद्धा-भक्ति होगी तो वह ब्रह्मलोक तक के लोकों को प्राप्त हो जायगा।
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा।
कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय।। 72।।
हे पृथानन्दन! क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय! क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ?
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्घा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।
स्थितोऽसिम गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।। 73।।
अर्जुन बोले-हे अच्युत! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं सन्देह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।
व्याख्या-लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्त्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है। इस तत्त्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात् अनुभव को ही यहाँ ‘स्मृतिर्लब्धा’ कहा गया है।
वास्तव में तत्त्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुखता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गयी-इस तरह तत्त्व की विस्मृति नहीं होती। यदि ऐसी विस्मृति मानें तो स्मृति होने के बाद पुनः विस्मृति हो जायगी। इसलिये गीता में आया है-‘यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्’ (4/35) अर्थात् उसे जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत् को भाव रूप मानकर महत्त्व देने से तत्त्व की तरफ से वृत्ति हट गयी-इसी को ‘विस्मृति’ कह देते हैं। वृत्ति का हटना अथवा लगना भी साधक की दृष्टि से वृत्ति हटे अथवा लगे, तत्त्व ज्यों-क्यों-त्यों ही रहता है। अभाव रूप असत् को अभाव रूप ही मान लें तो भाव यप तत्त्व स्वतः ज्यों-का-त्यों रह जाता है।
जीव अनादिकाल से स्वतः परमात्मा का है। उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन हैं, पर भक्तियोग साध्य है। इसलिये भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है। भक्ति योग साध्य है। भक्तियोग की स्मृति है-‘वासुदेव’ (गीता 7/19)। अतः एक वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं है-इसका अनुभव होना ही ‘स्मृतिर्लब्धा है। यह अनुभव केवल भगवत्कृपा से ही होता है-‘त्वत्प्रासादात्’। वचन सीमित होते हैं, पर कृपा असीम होती है।-क्रमशः (हिफी)