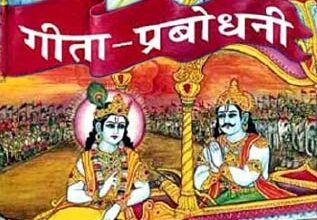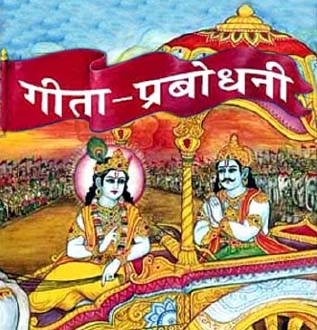
जिस तरह मर्यादा पुुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र को लेकर कहा गया है कि ‘हरि अनंत हरि कथा अनंता…’ उसी प्रकार भगवान कृष्ण के मुखार बिन्दु से प्रस्फुटित हुई श्रीमद् भगवत गीता का सार भी अतल गहराइयों वाला है। विद्वानों ने अपने-अपने तरह से गीता के रहस्य को समझने और समझाने का प्रयास किया है। गीता का प्रारंभ ही जिस श्लोक से होता है उसकी गहराई को समझना आसान नहीं है। कौरवों और पांडवों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वह भी धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म भूमि और कुरु क्षेत्रे अर्थात तीर्थ भूमि पर लड़ा गया जिससे युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वालों का कल्याण हो गया। इसी तरह की व्याख्या स्वामी रामसुख दास ने गीता प्रबोधनी में की है जिसे हम हिफी के पाठकों के लिए क्रमशः प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। हम स्वामी जी के आभारी हैं जिन्होंने गीता के श्लोकों की सरल शब्दों में व्याख्या की है। -प्रधान सम्पादक
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के दिन और रात
सहóयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः।
रात्रिं युगसहस्त्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः।। 17।।
जो मनुष्य ब्रह्मा के एक हजार चतुर्युगी वाले एक दिन को और एक हजार चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं।
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके।। 18।।
ब्रह्मा के दिन के आरम्भ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सम्पूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात आरम्भ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही सम्पूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं।
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे।। 19।।
हे पार्थ! वही यह प्राणि समुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है।
व्याख्या-बदलने वाले शरीर-संसार का विभाग अलग है और न बदलने वाले आत्मा-परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर-संसार तो बार-बार उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, पर आत्मा-परमात्मा वैसे-के-वैसे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय-महाप्रलय और सर्ग-महासर्ग क्यों न हो जायँ, जीवात्मा स्वयं वही का वही रहता है। इसलिये देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परन्तु शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिये मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार-बार जन्मता-मरता रहता है।
जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, जहाँ रेलगाड़ी जायगी, वहाँ उसे जाना ही पड़ता है, ऐसे ही शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म-मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है।
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः।
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति।। 20।।
परन्तु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यन्त श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह सम्पूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता।
व्याख्या-ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है (गीता 19/43)। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न हो-होकर लीन हो गये, पर परमात्मा वैसे-के-वैसे ही हैं।
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते त˜ाम परमं मम।। 21।।
उसी को अव्यक्त और अक्षर जैसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है।
व्याख्या-वास्तव में परमात्मतत्त्व वर्णनातीत है। अव्यक्त, अक्षर, परमगति आदि नाम उस तत्त्व का संकेत मात्र करते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त-व्यक्त, अक्षर-क्षर, गति-स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्त्व है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता है। कारण कि जीव उस परमात्मतत्त्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में जो वह भूल से अपने को स्थित मानता है। वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं।
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।। 22।।
हे पृथानन्दन अर्जुन! सम्पूर्ण प्राणी जिसके अन्तर्गत हैं और जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है।
व्याख्या-ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है परन्तु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ-साथ भक्त को भगवान् की तथा उनके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन हैं और भक्ति योग
साध्य है।
यत्र काले त्वनावृृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।। 23।।
परन्तु हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन! जिस काल अर्थात् मार्ग में शरीर छोड़कर गये हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात् पीछे लौटकर नहीं आते और जिस मार्ग में गये हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात् पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात् दोनों मार्गों को मैं कहूँगा।
व्याख्या-जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु कपड़ा, थैला, रुपये आदि छूट जाती है तो उसे लेने के लिये हम वापस उस स्थान पर जाते हैं, ऐसे ही संसार में किसी वस्तु-व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर-संसार के साथ सम्बन्ध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है और शरीर-संसार के साथ सम्बन्ध न रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता।-क्रमशः (हिफी)