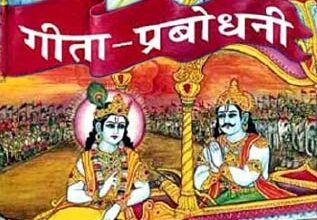श्रीमद् भगवत गीता का प्रबोध-96
जिस तरह मर्यादा पुुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र को लेकर कहा गया है कि ‘हरि अनंत हरि कथा अनंता…’ उसी प्रकार भगवान कृष्ण के मुखार बिन्दु से प्रस्फुटित हुई श्रीमद् भगवत गीता का सार भी अतल गहराइयों वाला है। विद्वानों ने अपने-अपने तरह से गीता के रहस्य को समझने और समझाने का प्रयास किया है। गीता का प्रारंभ ही जिस श्लोक से होता है उसकी गहराई को समझना आसान नहीं है। कौरवों और पांडवों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वह भी धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म भूमि और कुरु क्षेत्रे अर्थात तीर्थ भूमि पर लड़ा गया जिससे युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वालों का कल्याण हो गया। इसी तरह की व्याख्या स्वामी रामसुख दास ने गीता प्रबोधनी में की है जिसे हम हिफी के पाठकों के लिए क्रमशः प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। हम स्वामी जी के आभारी हैं जिन्होंने गीता के श्लोकों की सरल शब्दों में व्याख्या की है। -प्रधान सम्पादक
ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा।
कर्तुं नेच्छसि यम्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्।। 60।।
हे कुन्ती नन्दन्! अपने स्वभावजन्य कर्म से बँधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू (क्षात्र-प्रकति के) परवश होकर करेगा।
व्याख्या-भगवान् कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा न मानने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बाँधने वाला हो जायगा। परन्तु मेरी आज्ञा मानकर विहित कर्म करने से वह कर्म तेरे लिये कल्याणकारी हो जायेगा।
जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति (स्वभाव) महान् शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुष भी जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है (गीता 3/33), फिर प्रकृति के परवश हुआ अशुद्ध प्रकति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुष्ज्ञ कर्म कैसे कर सकता है?
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।। 61।।
हे अर्जुन! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यन्त्र पर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियों को (उनके स्वभाव के अनुसार) भ्रमण कराता रहता है।
व्याख्या-जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, पालक एवं संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियां को घुमाता है, जिन्होंने शरीर को ‘मैं’ और ‘मेरा’ मान रखा है। जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवशता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है, ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यन्त्र के साथ ‘मैं’ और ‘मेरे’ पन का सम्बन्ध मानता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म-मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मैं-मेरे पन का सम्बन्ध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।। 62।।
हे भरत वंशो˜व अर्जुन! तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शान्ति (संसार से सर्वथा उपरति) को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जायगा।
व्याख्या-जीव ईश्वर का ही अंश है-‘ईस्वर अंस जीव अबिनासी’ (मानस, उत्तर0 117/1), ‘ममैवांशो जीवलोके’ (गीता 15/7)। इसलिये भगवान् ईश्वर की ही शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश (शरण) में नहीं होता, तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है।
सबके हृदय में अन्तर्यामी-रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान् श्रीकृष्ण हैं, और भगवान् श्रीकृष्ण ही सबके हृदय में अन्तर्यामी रूप से स्थित ईश्वर हैं (गीता 4/6, 5/29, 8/4, 9/24, 15/14)।
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया।
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।। 63।।
यह गुह्य से भी गुह्यतर (शरणागति रूप) ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है, वैसा कर।
व्याख्या-तू जैसा चाहता है, वैसा कर-इस कथन में भगवान् की विशेष आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता भरी हुई है। ये वचन भगवान् अर्जुन का त्याग करने के लिये नहीं कहते हैं, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिये कहते हैं, जैसे-गेंद फंेकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिये, न कि त्याग करने के लिये। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अन्र्तयामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान् अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात् सगुण-सार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित न रह जाय। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है।
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः।
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।। 64।।
सबसे अत्यन्त गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र है, इसलिये यह (विशेष) हित की बात मैं तुझे कहूँगा।
व्याख्या-कर्मयोग ‘गुह्य’ है (गीता 4/3), अन्तर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति ‘गुह्यतर’ है (गीता 18/63), परमात्मा के प्रभाव की बात ‘गुह्यतम’ है (गीता 9/1, 15/20) और साकार परमात्मा की शरणागति ‘सर्वगुह्यतम’ है। यह ‘सर्वगुह्यतमम्’ पद गीता में एक ही बार यहाँ आया है।
निराकार की शरण में जाने से मुक्ति हो जाती है, पर साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ-साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान् ने भक्ति के प्रसंग में ही ‘परम वचन’ कहे हैं (गीता 10/1)।
अर्जुन ने भगवान् से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ-‘शिष्यस्तेऽहम’ (2/7), पर भगवान् यहाँ कहते हैं कि तू मेरा प्रिय मित्र है-‘इष्टोऽसि’। तात्पर्य है कि भगवान् अपने को गुरू न मानकर मित्र ही मानते हैं। भगवान् सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। यह सिद्धांत है कि जो खुद छोटा होता है, वही दूसरे को छोटा बनाता है। भगवान् सबसे बड़े हैं, इसलिये वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते।
मन्मना भव भ˜क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। 65।।
तू मेरा भक्त हो जा, मुझमें मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जायगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है।
व्याख्या-भगवान् का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना-इन चारों में एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन स्वतः में आ जाते हैं। भगवान् का भक्त होने का तात्पर्य है-‘मैं भगवान् का ही हूँ’ इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। भगवान् में मन लगाने का तात्पर्य है-भगवान् को अपना मानना। भगवान् को नमस्कार करने का तात्पर्य है-अपने-आपको भगवान् के समर्पित करना।-क्रमशः (हिफी)